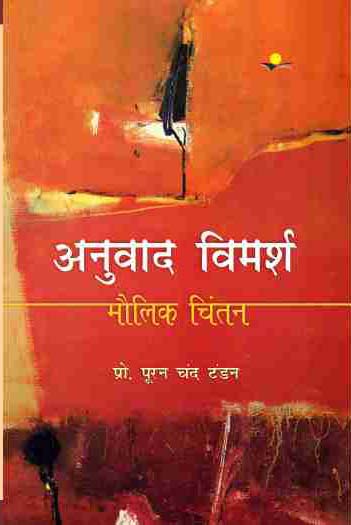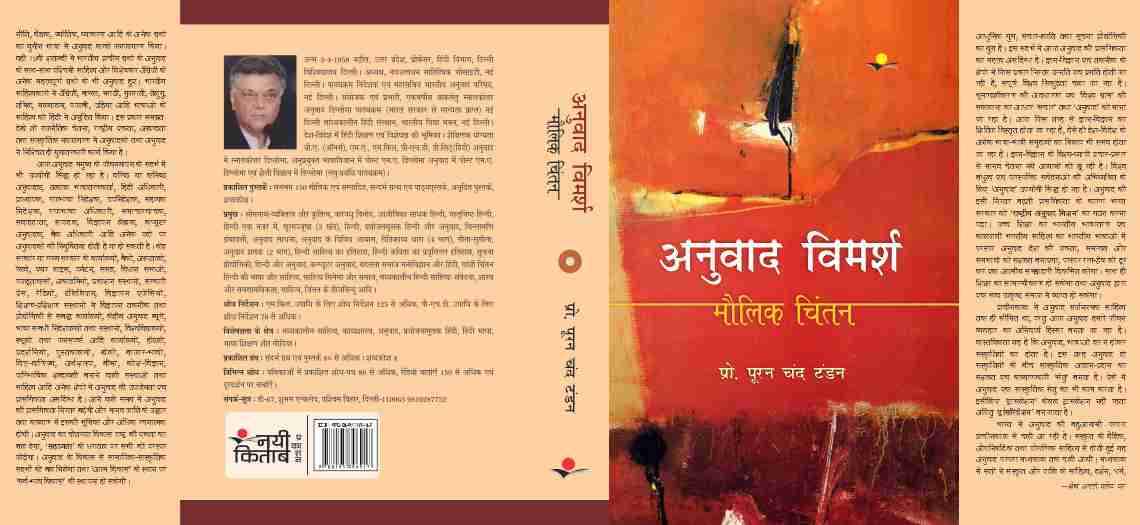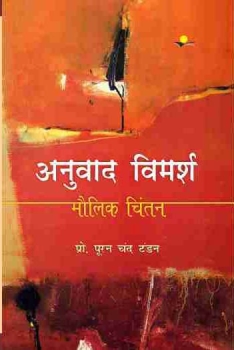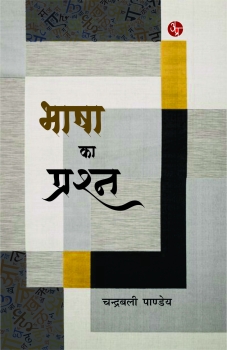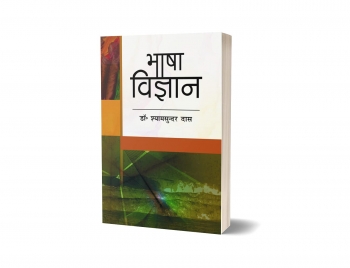- New product
Anuvaad Vimarsh : Molik Chintan
आधुनिक युग, संचार–क्रांति तथा सूचना प्रौद्योगिकी का युग है । इस संदर्भ में आज अनुवाद की प्रासंगिकता का महत्त्व असंदिग्ध है । ज्ञान–विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्रों में जिस प्रकार निरंतर उन्नति एवं प्रगति होती जा रही है, संपूर्ण विश्व सिकुड़ता चला जा रहा है । भूमंडलीकरण की अवधारणा एवं ‘विश्व ग्राम’ की संकल्पना का आधार ‘संचार’ तथा ‘अनुवाद’ को माना जा रहा है । आज जिस तरह से ज्ञान–विज्ञान का क्षितिज विस्तृत होता जा रहा है, वैसे ही देश–विदेश के अनेक भाषा–भाषी समुदायों का मिलाप भी संभव होता जा रहा है । ज्ञान–विज्ञान के विश्व–व्यापी प्रचार–प्रसार से मानव चेतना नये आयामों को छू रही है । विश्व बंधुत्व एवं पारस्परिक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए ‘अनुवाद’ उपयोगी सिद्ध हो रहा है । अनुवाद की इसी निरंतर बढ़ती प्रासंगिकता के कारण भारत सरकार को ‘राष्ट्रीय अनुवाद मिशन’ का गठन करना पड़ा । उच्च शिक्षा का भारतीय भाषांतरण एवं कालजयी भारतीय साहित्य का भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद देश की एकता, समन्वय और समभावों को सशक्त बनाएगा, परस्पर राग–द्वेष को दूर कर एक आत्मीय समझदारी विकसित करेगा । साथ ही शिक्षा का सामान्यीकरण हो सकेगा तथा अनुवाद द्वारा एक भाव उत्कृष्ट समाज में व्याप्त हो सकेगा । प्राचीनकाल में अनुवाद सर्जनात्मक साहित्य तक ही सीमित था, परंतु आज अनुवाद हमारे जीवन व्यवहार का अनिवार्य हिस्सा बनता जा रहा है । वास्तविकता यह है कि अनुवाद, भाषाओं का न होकर संस्कृतियों का होता है । इस तरह अनुवाद दो संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान का सशक्त एवं कल्याणकारी ‘सेतु’ बनता है । ऐसे में अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु का भी काम करता है । इसीलिए ‘ट्रांसलेशन’ केवल ट्रांसलेशन नहीं रहता अपितु ‘ट्रांसरिलेशन’ बन जाता है । भारत में अनुवाद की बहुआयामी परंपरा प्राचीनकाल से चली आ रही है । संस्कृत के वैदिक, औपनिषदिक तथा पौराणिक साहित्य से होती हुई यह अनुवाद परंपरा मध्यकाल तक चली आयी । मध्यकाल में संतों ने संस्कृत और पालि के साहित्य, दर्शन, धर्म, नीति, वैद्यक, ज्योतिष, व्याकरण आदि के अनेक ग्रंथों का युगीन भाषा में अनुवाद करके जनजागरण किया । वहीं 19वीं शताब्दी में भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद के साथ–साथ पश्चिमी साहित्य और विशेषकर अँग्रेज“ी के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथों के भी अनुवाद हुए । भारतीय साहित्यकारों ने अँग्रेज“ी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, उड़िया आदि भाषाओं के साहित्य को हिंदी में अनूदित किया । इस प्रकार समग्रत% देखें तो राजनैतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता तथा सांस्कृतिक नवजागरण में अनुवादकों तथा अनुवाद ने निश्चित ही युगांतरकारी कार्य किया है । आज अनुवाद मनुष्य के जीवनयापन के संदर्भ में भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है । वरिष्ठ या कनिष्ठ अनुवादक, तत्काल भाषांतरणकर्ता, हिंदी अधिकारी, प्राध्यापक, राजभाषा निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, राजभाषा अधिकारी, समाचारवाचक, संवाददाता, संपादक, विज्ञापन लेखक, कंप्यूटर अनुवादक, बैंक अधिकारी आदि अनेक पदों पर अनुवादकों की नियुक्तियां होती हैं या हो सकती हंै । केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों, बैंकों, अस्पतालों, रेलवे, एयर लाइंस, पर्यटन, संसद, विधान सभाओं, राजदूतावासों, अकादमियों, प्रकाशन संस्थानों, सरकारी प्रेस, रेडियो, टेिलविज“न, विज्ञापन एजेंसियों, शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों में विज्ञापन तकनीक तथा प्रौद्योगिकी से संबद्ध कार्यालयों, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, भाषा संबंधी निदेशालयों तथा संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों तथा जनसंपर्क आदि कार्यालयों, होटलों, प्रदर्शनियों, पुस्तकालयों, खेलों, बाजार–भावों, वित्त–वाणिज्य, अर्थशास्त्र, बीमा, कोश–विज्ञान, पारिभाषिक शब्दावली बनाने वाली संस्थाओं तथा साहित्य आदि अनेक क्षेत्रों में अनुवाद की उपादेयता एवं प्रासंगिकता असंदिग्ध है । आने वाले समय में अनुवाद की प्रासंगिकता निरंतर बढ़ेगी और मानव जाति के उद्धार तथा कल्याण में इसकी भूमिका और अधिक रचनात्मक होगी । अनुवाद का चैतरफा विकास राष्ट्र की एकता का बल देगा, ‘सहृदयता’ के धरातल पर सभी को परस्पर जोड़ेगा । अनुवाद के विकास से सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भों को बल मिलेगा तथा ‘आत्म विकास’ के स्थान पर ‘सर्व–भाव विकास’ की स्थापना हो सकेगी ।